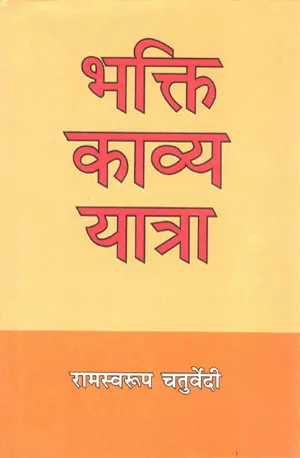|
लेख-निबंध >> शरत् के नारी पात्र शरत् के नारी पात्ररामस्वरूप चतुर्वेदी
|
263 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है शरत के नारी पात्रों का उनकी रचनाओं के आधार पर आलोचनात्मक अध्ययन...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
इस पीढ़ी का कौन पाठक ऐसा है जो शरत् के नारी-पात्रों से अपरिचित होगा।
श्रीकान्त के घुमक्क्ड़ जीवन की केन्द्रबिन्दु असीम स्नेहमयी राजलक्ष्मी,
वृन्दावन जाती हुई लांछिता कमललता, देवदास की पारो, गृहदाह में दो मित्रों
के बीच भटकती हुई अचला, असीम वात्सल्यमयी बिन्दो- इन स्नेह, करुणा, ममता
और मर्यादा से निर्मित शब्दमूर्तियों की एक पूरी पंक्ति हमारी मन की आँखों
के सामने से गुज़र जाती है। हर पाठक ने व्यथा के क्षणों के शरत् के इन
पात्रों से ममता पाई है, सान्त्वना पाई है। वे हमारे जीवन के अभिन्न अंग
बन चुके हैं।
शरत् के इन अमर नारी-पात्रों का सूक्ष्म और सहानुभूति विश्लेषण डाँ.रामस्वरूप चतुर्वेदी ने प्रस्तुत किया है कई भारतीय भाषाओं में अनूदित और चर्चित होकर यह कृति सामान्य पाठकों और विदग्ध समीक्षकों के बीच शरत् के साथ-साथ घूमी है। अब प्रस्तुत हैं इस आलोचना कृति का नया संस्करण एक विस्तृत और अभिनव भूमिका के साथ, जिनका शीर्षक है ‘भारतीय आलोचना : बांग्ला और हिन्दी साहित्य के संपर्क की पृष्ठभूमि में’। यह भूमिका मूल ग्रन्थ को, उसके उपजीव्य के साथ, फिर सही परिप्रेक्ष्य में रखती है।
जिससे बांग्ला साहित्य के अध्ययन की प्रेरणा मिली तथा शरतचन्द्र के उन सभी वास्तविक-अवास्तविक चरित्रों को जिन्होंने जीवन के मर्म को अधिकाधिक समझ सकने के प्रयत्न में सहयोग दिया है।
‘‘सुसभ्य मनुष्य की स्वस्थ, संयत तथा शुभ बुद्धि नारी जाति को अधिकार अर्पित करने के लिए कहती है, वही मनुष्य की सामाजिक नीति है और उसी से समाज का कल्याण होता है। समाज का कल्याण इस बात से नहीं होता कि किसी जाति की धर्म-पुस्तक में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। नारी के मूल्य का विवेचन करते हुए हम अब तक इसी नीति और इसी अधिकार की बात कहते आये हैं। हमने supply और demand अर्थात् उपज और माँग की कीमत भी नहीं कही और यह आशा भी नहीं की कि कोई ऐसा समय आएगा, जबकि पुरुषों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी और स्त्रियाँ बिलकुल विरल हो जाएँगी। नारी का मूल्य निर्भर करता है पुरुष के स्नेह, सहानुभूति और न्याय-धर्म पर। भगवान ने उसे दुर्बल ही बनाया है और पुरुष उसके बल के इस अभाव की पूर्ति ऊपर बतलाई हुई वृत्तियों की ओर देखकर ही कर सकता है धर्म-पुस्तकों की बातों की बाल की खाल निकालकर उनके अबोध्य अर्थों की सहायता से उसकी पूर्ति नहीं कर सकता।’’
शरत् के इन अमर नारी-पात्रों का सूक्ष्म और सहानुभूति विश्लेषण डाँ.रामस्वरूप चतुर्वेदी ने प्रस्तुत किया है कई भारतीय भाषाओं में अनूदित और चर्चित होकर यह कृति सामान्य पाठकों और विदग्ध समीक्षकों के बीच शरत् के साथ-साथ घूमी है। अब प्रस्तुत हैं इस आलोचना कृति का नया संस्करण एक विस्तृत और अभिनव भूमिका के साथ, जिनका शीर्षक है ‘भारतीय आलोचना : बांग्ला और हिन्दी साहित्य के संपर्क की पृष्ठभूमि में’। यह भूमिका मूल ग्रन्थ को, उसके उपजीव्य के साथ, फिर सही परिप्रेक्ष्य में रखती है।
जिससे बांग्ला साहित्य के अध्ययन की प्रेरणा मिली तथा शरतचन्द्र के उन सभी वास्तविक-अवास्तविक चरित्रों को जिन्होंने जीवन के मर्म को अधिकाधिक समझ सकने के प्रयत्न में सहयोग दिया है।
‘‘सुसभ्य मनुष्य की स्वस्थ, संयत तथा शुभ बुद्धि नारी जाति को अधिकार अर्पित करने के लिए कहती है, वही मनुष्य की सामाजिक नीति है और उसी से समाज का कल्याण होता है। समाज का कल्याण इस बात से नहीं होता कि किसी जाति की धर्म-पुस्तक में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। नारी के मूल्य का विवेचन करते हुए हम अब तक इसी नीति और इसी अधिकार की बात कहते आये हैं। हमने supply और demand अर्थात् उपज और माँग की कीमत भी नहीं कही और यह आशा भी नहीं की कि कोई ऐसा समय आएगा, जबकि पुरुषों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी और स्त्रियाँ बिलकुल विरल हो जाएँगी। नारी का मूल्य निर्भर करता है पुरुष के स्नेह, सहानुभूति और न्याय-धर्म पर। भगवान ने उसे दुर्बल ही बनाया है और पुरुष उसके बल के इस अभाव की पूर्ति ऊपर बतलाई हुई वृत्तियों की ओर देखकर ही कर सकता है धर्म-पुस्तकों की बातों की बाल की खाल निकालकर उनके अबोध्य अर्थों की सहायता से उसकी पूर्ति नहीं कर सकता।’’
शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय
भारतीय आलोचना :
बांग्ला और हिन्दी साहित्य के सम्पर्क की पृष्ठिभूमि में
भारत संघ का राजभाषा या कि समपर्क-भाषा बनने के बहुत पहले से
हिन्दी
सभी भारतीय भाषाओं को जोड़ने का काम करती आयी है। इस रूप में हिन्दी
क्षेत्र समस्त भारतवर्ष का हृदय-स्थल कहा जा सकता है, न केवल भौगोलिक अथवा
शुद्ध भावात्मक दृष्टि से बल्कि रूपक और प्रमाणित करते हुए समस्त संस्कृति
का संचयन करने की दृष्टि से। हृदय सम्पूर्ण शरीर में रक्त-संचार का माध्यम
है। हिन्दी क्षेत्र (या प्राचीन मध्यदेश) समूचे भारतवर्ष में राष्ट्रीय
संस्कृति का संचार करता रहा है, एक प्रदेश के विचारों-अनुभवों का संक्रमण
दूसरे प्रदेश में करता हुआ। कुछ वर्ष हिन्दी में अनूदित उपन्यास-साहित्य
पर एक शोध-कार्य देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। शोध-कर्ता ने वहां तथ्यों
और आँकड़ों के सहारे दिखाया था कि हिन्दी में सारी आधुनिक भारतीय भाषाओं
से उपन्यासों के अनुवाद हुए हैं, संख्या की दृष्टि से बांग्ला के
सार्वधिक।
इसके साथ ही एक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष उस अध्ययन से यह भी निकलता था कि अनेक भाषाओं में अनुवाद सीधे न होकर हिन्दी के माध्यम से हुए हैं, यानि कोई बांग्ला उपन्यास मराठी या कि गुजराती में सीधे बांग्ला से न होकर हिन्दी अनुवाद के माध्यम से आया है। स्पष्ट ही इन सभी प्रकार के अनुवादों के आधार पर- वे चाहे उपन्यास के हों, या कविता के, या नाटक के- भारतीय साहित्य की अवधारणा बनती है। बंकिम, रवीन्द्र, प्रेमचन्द्र, क.मा.मुंशी, वि.स. खाण्डेकर, सुब्रह्मण्य भारती, बांग्ला, हिन्दी, गुजराती, मराठी, तमिल लेखक तो हैं ही, साथ ही उनका भारतीय चरित्र और परिवेश भी इस रूप में उभरता है।
पिछले कुछ समय से इस संदर्भ में यह सजगता बढ़ी है कि आलोचना के परिदृश्य पर हम भारतीय पाठक रिचर्ड्स, एलियट, सार्त्र, रोलाँ बार्थ या कि डैवीडोव के विचारों, सिद्धान्तों से तो परिचित हैं, उन पर अधिकारपूर्वक विवेचन भी करते हैं, पर मर्ढेकर, टोपीवाला, रामचन्द्र शुक्ल, कारंथ और बुद्धदेव बसु के साहित्य-चिंतन से हम प्रायः अपरिचित हैं।
होना यह चाहिए था कि भारतीय साहित्य की अवधारणा को आगे विकसित करने में आलोचना का गुणात्मक योग होता, पर अनेक कारणों से आलोचना की यह भूमिका बहुत कम गतिशील हुई। यहाँ आलोचना का दायित्व वस्तुतः दोहरा बनता है। एक ओर तो एक साहित्य के लेखक पर दूसरे साहित्य के आलोचक द्वारा लिखे जाने से समझादारी का सेतु बनता और प्रशस्त होता। दूसरी ओर समूचे भारतीय साहित्य के परिदृश्य पर हुए आलोचनात्मक चिन्तन पर समग्र रूप से विचार-विमर्श चलता। यहाँ स्मरणीय हैं कि ‘आलोचना’ पद का प्रयोग ही इस दृष्टि से है कि प्रस्तुत विवेचन के केन्द्र में आधुनिक साहित्य है। संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय साहित्यों के सन्दर्भ में इस अनुशासन के लिए ‘काव्यशास्त्र’ प्रयोग समीचीन होगा। इस दृष्टि से ‘भारतीय आलोचना’ का अर्थ और सन्दर्भ आप से आप आधुनिक कान से जुड़ जाता है, जो प्रायः समूचे भारतीय परिदृश्य पर 19 वीं शती का आरम्भ माना जाता है।
भारतीय आलोचना की उपर्युक्त दो प्रक्रियाओं में से ‘शरत् के नारी पात्र’ (1955) का संबंध पहली प्रक्रिया से जुड़ता है, अर्थात् जहाँ एक भारतीय साहित्य का समीक्षक दूसरे भारतीय साहित्य के लेखक की रचनात्मकता को अपनी आलोचना का उपजीव्य बनाता है। हिन्दी पाठक का बांग्ला साहित्य से सम्पर्क एक प्रकार से वह बिन्दु है जहाँ से इस रूप में भारतीय साहित्य और भारतीय आलोचना का सूत्रपात होता है। माईकेल मधुसूदन और रवीन्द्र का काव्य, बंकिम तथा शरत् के उपन्यास, द्विजेन्द्रलाला राय से लेकर बादल सरकार के नाटक दो भारतीय भाषा-क्षेत्रों के बीच आरम्भिक सेतु का कार्य करते दिखते हैं। पुनर्जागरण काल से आरम्भ में 19वीं शती से ही हिन्दी क्षेत्र के निवासियों की बंगाल की ओर उन्मुखता से यह सम्पर्क संभव होता है; कलकत्ता उस समय तत्त्कालीन व्यावसायिक तथा इस सांस्कृतिक उन्मेष का केन्द्र बनता है। बांग्ला ही नहीं, आधुनिक हिन्दी साहित्य, पत्रकारिता तथा प्रकाशन-क्षेत्र की सक्रियता भी कुछ वहीं से आरम्भ होती है। यह संयोग नहीं कि ‘शरत् के नारी पात्र’ के उपजीव्य लेखक, आलोचक तथा प्रकाशक तीनों का कलकत्ता नगर से कम-बढ़ सम्बन्ध रहा है। हिन्दी क्षेत्र की बंगाल से यह रचनात्मक स्तर पर क्रिया-प्रतिक्रिया अनेक रूपों में फलप्रद हुई है।
रवीन्द्रनाथ का, और रवीन्द्रनाथ से निराला का सम्पर्क इस स्तर पर प्रतीक रूप में श्रेष्ठतम उपलब्धियों का उत्प्रेरक कहा जा सकता है।
प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रकाशन-संस्था भारतीय ज्ञानपीठ ने अपना विस्तृत कार्यारम्भ कलकत्ता में किया। ब्रिटिशकालीन राजधानी की तरह दिल्ली वह बाद में पहुँची। अपने नाम के अनुरूप पहले उनका ध्यान भारत के परम्परागत वाङ्मय की ओर अधिक रहा, झुकाव समकालीन साहित्य की ओर होता गया, जहाँ भारतीय साहित्य की परिकल्पना अभी बहुत उभर कर नहीं आयी थी। ‘शरत् के नारी पात्र’ अध्ययन जब प्रकाशित हुआ 1955 में तब वह ज्ञानपीठ की लोकोदय ग्रन्थमाला में बयालीसवाँ ग्रन्थ था- अब यह ग्रन्थांक 1993 में पाँच सौ पचास को पार गया है- और उर्दू शायरी के सीमित सन्दर्भ को छोड़कर किसी अन्य समकालीन भारतीय पर उनका कोई प्रकाशन नहीं था।
हिन्दी आलोचना में भी इस प्रकार के अन्तःप्रादेशिक साहित्यिक सम्पर्क को चरित्र-परिकल्पना की सूक्ष्म दृष्टि से सक्रिय करने वाला कोई व्यवस्थित ग्रन्थ था, नहीं कह सकता। रवीन्द्र-काव्य की कुछ व्याख्याएँ जरूर थीं, जिनमें निराला का ‘रवीन्द्र कविता कानन’ सहज स्मरण हो आता है। तथा शरत्-साहित्य पर कुछ परिचयात्मक-आलोचनात्मक पुस्तकें थीं। फिर, जैसा कहा गया है, स्वयं ज्ञानपीठ का रुझान कई स्तरों पर भारतीय साहित्य की परिकल्पना को विकसित और पुरस्कृत करने में बढ़ा, जिसके व्यावहारिक रूप में उत्साहवर्धक परिणाम सामने आये। ज्ञानपीठ पुरस्कार की संस्थापना ने- जिसकी रजत जयन्ती तीन वर्ष पूर्व मनायी जा चुकी है- समूचे भारतीय साहित्य को पहली बार एक साथ मूल्यांकित करने का महत्त्वपूर्ण प्रयास किया। इस पुरस्कार की धन-राशि (आरम्भ में एक लाख, अब दो लाख) अपनी जगह थी, पर इनकी चयन-प्रक्रिया ने इसे और स्मरणीय तथा विश्वसनीय बनाया।
किसी भी पुरस्कार की मर्यादा को बनाने में ये दो तत्त्व प्रधान होते हैं, और इन दोनों ही स्तरों पर ज्ञानपीठ पुरस्कार उत्तरोत्तर महिमामण्डित होता गया है, साथ-साथ भारतीय साहित्य की व्यापक परिकल्पना को और सुदृढ़ बनाता गया है। व्यावहारिक स्तर पर इस पुरस्कार के माध्यम से ज्ञानपीठ भारतीय भाषाओं के अनेक समकालीन क्लासिकों को प्रकाशित कर सका है। इसके अतिरिक्त इधर स्वतंत्र रूप से भी उन्होंने ‘भारतीय कवि’ ‘भारतीय कथाकार’ आदि मालाओं के अन्तर्गत विविध भाषाओं की महत्त्वपूर्ण रचनाओं का प्रकाशन आरम्भ किया है। ज्ञानपीठ के अतिरिक्त साहित्य अकादेमी, नेशनल बुक ट्रस्ट तथा भारत सरकार के प्रकाशन-विभाग ने केन्द्रीय सहायता से भारतीय भाषाओं के साहित्य को एक से दूसरी भाषा में प्रस्तुत किया है। काफी पहले प्रेमचन्द्र द्वारा संस्थापित पत्र ‘हंस’, उत्तरप्रदेश हिन्दी सीमित, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद जैसी संस्थाओं ने भारतीय भाषा तथा साहित्य के अलग-अलग परिचय-वृत्त प्रकाशित किये थे। अभी हाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग ने मेरे सुझाव पर भारतीय साहित्य के व्यवस्थित अध्ययन का प्रारूप प्रस्तुत करके वैदुषिक क्षेत्र में ऐसी पहल की है।
इस सन्दर्भ में अब भारतीय आलोचना की परिकल्पना को प्रसरित होने के लिए विस्तृत अवसर तथा व्यापक क्षेत्र मिल रहा है। इस दिशा में अग्रणी अध्ययन डॉ. नगेन्द्र द्वारा सम्पादित हुआ है ‘भारतीय समीक्षा’ (1975)। अलग-अलग साहित्यों में समीक्षा अथवा आलोचना के विकास को दरसाने वाले निबन्ध यहाँ संकलित हैं सम्पादक की विस्तृत भूमिका के साथ, जहाँ भारतीय समीक्षा के व्यापक रूप को प्रकट करने का यत्न हुआ है। नगेन्द्र के प्राचीन भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र के ऐसे ही अध्ययनों के क्रम में उनकी यह पुस्तक इस सन्दर्भ में प्रस्तुत करती है, पर उससे ऊपर नहीं उठ पाती। यह संभवतः उसका क्षेत्र नहीं, और सम्पादक की रुचि की यह सीमा भी है। व्यावहारिक आलोचना के क्षेत्र में कार्यशील रहने के बावजूद डॉ. नगेन्द्र का प्रधान क्षेत्र संस्कृत काव्यशास्त्र और सैद्धान्तिक आलोचना का रहा है। इसी पृष्ठभूमि में वे ‘भारतीय समीक्षा’ शीर्षक अपनी भूमिका में भारतीय समीक्षा की व्याख्या इस रूप में करते हैं- ‘‘भारतीय समीक्षा’’ का एक तीसरा अर्थ भी हो सकता है : विविध भाषाओं की सामान्य प्रवृत्तियों और उपलब्धियों की संहति ही ‘भारतीय समीक्षा’ है। इस परिभाषा के अनुसार ‘भारतीय समीक्षा’ उस समीक्षा-पद्धति का नाम है जो-
भारतीय भाषा-साहित्य के सन्दर्भ में संस्कृति और पाश्चात्य समीक्षा-तत्त्वों के समन्वय से विकसित हुई है;
प्रादेशिक अथवा प्रान्तीय साहित्य की विलक्षणताओं से मुक्त है;
सर्वदेशिक गुणों से मुक्त है;
और भारतीय साहित्य की समग्र चेतना को प्रतिफलित करती है।
मेरे विचार से यही अर्थ सर्वाधिक शुद्ध एवं संगत है, और इसी के आधार पर ‘भारतीय समीक्षा’ के स्वरूप का निर्णय और विकास-क्रम का निरूपण किया जा सकता है।’’
यहाँ डॉ. नगेन्द्र की उपर्युक्त परिभाषा तथा व्याख्या का विस्तृत विवेचन करने का अवसर नहीं है, फिर भी सामान्य रूप से यह तो कहा ही जा सकता है कि डॉ.नगेन्द्र ने भारतीय समीक्षा के अपने द्वारा गिनाये गये लक्षणों में जो दूसरा निर्देश किया है वह नितान्त आदेशात्मक है, शायद उनकी काव्यशास्त्रीय प्रकृति के अनुकूल। यदि प्रादेशिक साहित्य की विलक्षणताओं को परे कर दिया जाएगा तो भारतीय समीक्षा का जो स्वरूप विकसित होगा, वह नितान्त सामान्य कथनों का एक समुच्चय-मात्र होगा, और जो न प्रादेशिक साहित्य के वैशिष्ट्य को प्रकट करेगा और न उस वैशिष्ट्य का योगदान भारतीय आलोचना के स्वरूप में कर पाएगा। वैशिष्ट्य को सार्वजनीय बनाना साहित्य की प्रक्रिया है, और इसी प्रक्रिया का अगला चरण साहित्य की आलोचना या समीक्षा है।
इसके साथ ही एक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष उस अध्ययन से यह भी निकलता था कि अनेक भाषाओं में अनुवाद सीधे न होकर हिन्दी के माध्यम से हुए हैं, यानि कोई बांग्ला उपन्यास मराठी या कि गुजराती में सीधे बांग्ला से न होकर हिन्दी अनुवाद के माध्यम से आया है। स्पष्ट ही इन सभी प्रकार के अनुवादों के आधार पर- वे चाहे उपन्यास के हों, या कविता के, या नाटक के- भारतीय साहित्य की अवधारणा बनती है। बंकिम, रवीन्द्र, प्रेमचन्द्र, क.मा.मुंशी, वि.स. खाण्डेकर, सुब्रह्मण्य भारती, बांग्ला, हिन्दी, गुजराती, मराठी, तमिल लेखक तो हैं ही, साथ ही उनका भारतीय चरित्र और परिवेश भी इस रूप में उभरता है।
पिछले कुछ समय से इस संदर्भ में यह सजगता बढ़ी है कि आलोचना के परिदृश्य पर हम भारतीय पाठक रिचर्ड्स, एलियट, सार्त्र, रोलाँ बार्थ या कि डैवीडोव के विचारों, सिद्धान्तों से तो परिचित हैं, उन पर अधिकारपूर्वक विवेचन भी करते हैं, पर मर्ढेकर, टोपीवाला, रामचन्द्र शुक्ल, कारंथ और बुद्धदेव बसु के साहित्य-चिंतन से हम प्रायः अपरिचित हैं।
होना यह चाहिए था कि भारतीय साहित्य की अवधारणा को आगे विकसित करने में आलोचना का गुणात्मक योग होता, पर अनेक कारणों से आलोचना की यह भूमिका बहुत कम गतिशील हुई। यहाँ आलोचना का दायित्व वस्तुतः दोहरा बनता है। एक ओर तो एक साहित्य के लेखक पर दूसरे साहित्य के आलोचक द्वारा लिखे जाने से समझादारी का सेतु बनता और प्रशस्त होता। दूसरी ओर समूचे भारतीय साहित्य के परिदृश्य पर हुए आलोचनात्मक चिन्तन पर समग्र रूप से विचार-विमर्श चलता। यहाँ स्मरणीय हैं कि ‘आलोचना’ पद का प्रयोग ही इस दृष्टि से है कि प्रस्तुत विवेचन के केन्द्र में आधुनिक साहित्य है। संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय साहित्यों के सन्दर्भ में इस अनुशासन के लिए ‘काव्यशास्त्र’ प्रयोग समीचीन होगा। इस दृष्टि से ‘भारतीय आलोचना’ का अर्थ और सन्दर्भ आप से आप आधुनिक कान से जुड़ जाता है, जो प्रायः समूचे भारतीय परिदृश्य पर 19 वीं शती का आरम्भ माना जाता है।
भारतीय आलोचना की उपर्युक्त दो प्रक्रियाओं में से ‘शरत् के नारी पात्र’ (1955) का संबंध पहली प्रक्रिया से जुड़ता है, अर्थात् जहाँ एक भारतीय साहित्य का समीक्षक दूसरे भारतीय साहित्य के लेखक की रचनात्मकता को अपनी आलोचना का उपजीव्य बनाता है। हिन्दी पाठक का बांग्ला साहित्य से सम्पर्क एक प्रकार से वह बिन्दु है जहाँ से इस रूप में भारतीय साहित्य और भारतीय आलोचना का सूत्रपात होता है। माईकेल मधुसूदन और रवीन्द्र का काव्य, बंकिम तथा शरत् के उपन्यास, द्विजेन्द्रलाला राय से लेकर बादल सरकार के नाटक दो भारतीय भाषा-क्षेत्रों के बीच आरम्भिक सेतु का कार्य करते दिखते हैं। पुनर्जागरण काल से आरम्भ में 19वीं शती से ही हिन्दी क्षेत्र के निवासियों की बंगाल की ओर उन्मुखता से यह सम्पर्क संभव होता है; कलकत्ता उस समय तत्त्कालीन व्यावसायिक तथा इस सांस्कृतिक उन्मेष का केन्द्र बनता है। बांग्ला ही नहीं, आधुनिक हिन्दी साहित्य, पत्रकारिता तथा प्रकाशन-क्षेत्र की सक्रियता भी कुछ वहीं से आरम्भ होती है। यह संयोग नहीं कि ‘शरत् के नारी पात्र’ के उपजीव्य लेखक, आलोचक तथा प्रकाशक तीनों का कलकत्ता नगर से कम-बढ़ सम्बन्ध रहा है। हिन्दी क्षेत्र की बंगाल से यह रचनात्मक स्तर पर क्रिया-प्रतिक्रिया अनेक रूपों में फलप्रद हुई है।
रवीन्द्रनाथ का, और रवीन्द्रनाथ से निराला का सम्पर्क इस स्तर पर प्रतीक रूप में श्रेष्ठतम उपलब्धियों का उत्प्रेरक कहा जा सकता है।
प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रकाशन-संस्था भारतीय ज्ञानपीठ ने अपना विस्तृत कार्यारम्भ कलकत्ता में किया। ब्रिटिशकालीन राजधानी की तरह दिल्ली वह बाद में पहुँची। अपने नाम के अनुरूप पहले उनका ध्यान भारत के परम्परागत वाङ्मय की ओर अधिक रहा, झुकाव समकालीन साहित्य की ओर होता गया, जहाँ भारतीय साहित्य की परिकल्पना अभी बहुत उभर कर नहीं आयी थी। ‘शरत् के नारी पात्र’ अध्ययन जब प्रकाशित हुआ 1955 में तब वह ज्ञानपीठ की लोकोदय ग्रन्थमाला में बयालीसवाँ ग्रन्थ था- अब यह ग्रन्थांक 1993 में पाँच सौ पचास को पार गया है- और उर्दू शायरी के सीमित सन्दर्भ को छोड़कर किसी अन्य समकालीन भारतीय पर उनका कोई प्रकाशन नहीं था।
हिन्दी आलोचना में भी इस प्रकार के अन्तःप्रादेशिक साहित्यिक सम्पर्क को चरित्र-परिकल्पना की सूक्ष्म दृष्टि से सक्रिय करने वाला कोई व्यवस्थित ग्रन्थ था, नहीं कह सकता। रवीन्द्र-काव्य की कुछ व्याख्याएँ जरूर थीं, जिनमें निराला का ‘रवीन्द्र कविता कानन’ सहज स्मरण हो आता है। तथा शरत्-साहित्य पर कुछ परिचयात्मक-आलोचनात्मक पुस्तकें थीं। फिर, जैसा कहा गया है, स्वयं ज्ञानपीठ का रुझान कई स्तरों पर भारतीय साहित्य की परिकल्पना को विकसित और पुरस्कृत करने में बढ़ा, जिसके व्यावहारिक रूप में उत्साहवर्धक परिणाम सामने आये। ज्ञानपीठ पुरस्कार की संस्थापना ने- जिसकी रजत जयन्ती तीन वर्ष पूर्व मनायी जा चुकी है- समूचे भारतीय साहित्य को पहली बार एक साथ मूल्यांकित करने का महत्त्वपूर्ण प्रयास किया। इस पुरस्कार की धन-राशि (आरम्भ में एक लाख, अब दो लाख) अपनी जगह थी, पर इनकी चयन-प्रक्रिया ने इसे और स्मरणीय तथा विश्वसनीय बनाया।
किसी भी पुरस्कार की मर्यादा को बनाने में ये दो तत्त्व प्रधान होते हैं, और इन दोनों ही स्तरों पर ज्ञानपीठ पुरस्कार उत्तरोत्तर महिमामण्डित होता गया है, साथ-साथ भारतीय साहित्य की व्यापक परिकल्पना को और सुदृढ़ बनाता गया है। व्यावहारिक स्तर पर इस पुरस्कार के माध्यम से ज्ञानपीठ भारतीय भाषाओं के अनेक समकालीन क्लासिकों को प्रकाशित कर सका है। इसके अतिरिक्त इधर स्वतंत्र रूप से भी उन्होंने ‘भारतीय कवि’ ‘भारतीय कथाकार’ आदि मालाओं के अन्तर्गत विविध भाषाओं की महत्त्वपूर्ण रचनाओं का प्रकाशन आरम्भ किया है। ज्ञानपीठ के अतिरिक्त साहित्य अकादेमी, नेशनल बुक ट्रस्ट तथा भारत सरकार के प्रकाशन-विभाग ने केन्द्रीय सहायता से भारतीय भाषाओं के साहित्य को एक से दूसरी भाषा में प्रस्तुत किया है। काफी पहले प्रेमचन्द्र द्वारा संस्थापित पत्र ‘हंस’, उत्तरप्रदेश हिन्दी सीमित, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद जैसी संस्थाओं ने भारतीय भाषा तथा साहित्य के अलग-अलग परिचय-वृत्त प्रकाशित किये थे। अभी हाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग ने मेरे सुझाव पर भारतीय साहित्य के व्यवस्थित अध्ययन का प्रारूप प्रस्तुत करके वैदुषिक क्षेत्र में ऐसी पहल की है।
इस सन्दर्भ में अब भारतीय आलोचना की परिकल्पना को प्रसरित होने के लिए विस्तृत अवसर तथा व्यापक क्षेत्र मिल रहा है। इस दिशा में अग्रणी अध्ययन डॉ. नगेन्द्र द्वारा सम्पादित हुआ है ‘भारतीय समीक्षा’ (1975)। अलग-अलग साहित्यों में समीक्षा अथवा आलोचना के विकास को दरसाने वाले निबन्ध यहाँ संकलित हैं सम्पादक की विस्तृत भूमिका के साथ, जहाँ भारतीय समीक्षा के व्यापक रूप को प्रकट करने का यत्न हुआ है। नगेन्द्र के प्राचीन भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र के ऐसे ही अध्ययनों के क्रम में उनकी यह पुस्तक इस सन्दर्भ में प्रस्तुत करती है, पर उससे ऊपर नहीं उठ पाती। यह संभवतः उसका क्षेत्र नहीं, और सम्पादक की रुचि की यह सीमा भी है। व्यावहारिक आलोचना के क्षेत्र में कार्यशील रहने के बावजूद डॉ. नगेन्द्र का प्रधान क्षेत्र संस्कृत काव्यशास्त्र और सैद्धान्तिक आलोचना का रहा है। इसी पृष्ठभूमि में वे ‘भारतीय समीक्षा’ शीर्षक अपनी भूमिका में भारतीय समीक्षा की व्याख्या इस रूप में करते हैं- ‘‘भारतीय समीक्षा’’ का एक तीसरा अर्थ भी हो सकता है : विविध भाषाओं की सामान्य प्रवृत्तियों और उपलब्धियों की संहति ही ‘भारतीय समीक्षा’ है। इस परिभाषा के अनुसार ‘भारतीय समीक्षा’ उस समीक्षा-पद्धति का नाम है जो-
भारतीय भाषा-साहित्य के सन्दर्भ में संस्कृति और पाश्चात्य समीक्षा-तत्त्वों के समन्वय से विकसित हुई है;
प्रादेशिक अथवा प्रान्तीय साहित्य की विलक्षणताओं से मुक्त है;
सर्वदेशिक गुणों से मुक्त है;
और भारतीय साहित्य की समग्र चेतना को प्रतिफलित करती है।
मेरे विचार से यही अर्थ सर्वाधिक शुद्ध एवं संगत है, और इसी के आधार पर ‘भारतीय समीक्षा’ के स्वरूप का निर्णय और विकास-क्रम का निरूपण किया जा सकता है।’’
यहाँ डॉ. नगेन्द्र की उपर्युक्त परिभाषा तथा व्याख्या का विस्तृत विवेचन करने का अवसर नहीं है, फिर भी सामान्य रूप से यह तो कहा ही जा सकता है कि डॉ.नगेन्द्र ने भारतीय समीक्षा के अपने द्वारा गिनाये गये लक्षणों में जो दूसरा निर्देश किया है वह नितान्त आदेशात्मक है, शायद उनकी काव्यशास्त्रीय प्रकृति के अनुकूल। यदि प्रादेशिक साहित्य की विलक्षणताओं को परे कर दिया जाएगा तो भारतीय समीक्षा का जो स्वरूप विकसित होगा, वह नितान्त सामान्य कथनों का एक समुच्चय-मात्र होगा, और जो न प्रादेशिक साहित्य के वैशिष्ट्य को प्रकट करेगा और न उस वैशिष्ट्य का योगदान भारतीय आलोचना के स्वरूप में कर पाएगा। वैशिष्ट्य को सार्वजनीय बनाना साहित्य की प्रक्रिया है, और इसी प्रक्रिया का अगला चरण साहित्य की आलोचना या समीक्षा है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book